Rss यात्रा पर गर्व, लक्ष्य पाना शेष : दत्तात्रेय होसबाले

दिल्ली। Rss उगादी उत्सव के अवसर पर कन्नड़ साप्ताहिक विक्रम ने एक विशेषांक प्रकाशित किया ‘संघ शतपथ’। उस विशेषांक के लिए विक्रम के संपादक रमेश दोड्डपुरा ने रा.स्व.संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के साथ विशेष बातचीत की, जिसमें श्री होसबाले ने संघ और भावी कार्यों तथा समाज संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत हैं उस वार्ता के संपादित अंश।
संघ शाखा तंत्र की सफलता के पीछे क्या रहस्य है ? संघ ही वह संगठन है जो इस सरल और सुगठित तंत्र को स्थापित करने और उसे बनाए रखने में सफल रहा है। आपका क्या कहना है ?
संघ के संस्थापक पूज्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इससे उन्हें प्रगाढ़ अनुभव हुआ और यहीं से शाखा की अवधारणा और कार्यप्रणाली का जन्म हुआ। निश्चित ही, डॉ. हेडगेवार ने शाखा के बारे में गहराई से विचार किया होगा। शाखा सार्वजनिक स्थान पर खुले वातावरण में चलने वाली एक घंटे की दैनिक गतिविधि है। यह बहुत सरल और किसी भी प्रकार के रहस्य से दूर है। हालांकि, शाखा की संरचना सहज और सरल है, लेकिन इसका हिस्सा होने के लिए वर्षों तक शाखा में नियमित भागीदारी आवश्यक है। इससे यह थोड़ी जटिल प्रतीत होती है। शाखा का स्वयंसेवक होने के लिए व्यक्ति का निस्वार्थी होना और उसमें दृढ़ता और त्याग की भावना होना आवश्यक है। शाखा का आधार है स्वयंसेवकों में सौहार्द और भावनात्मक जुड़ाव। संघ की 100 वर्ष की यात्रा ने साबित कर दिया है कि यह सामाजिक संगठन और परिवर्तन का सबसे प्रभावी मॉडल है।
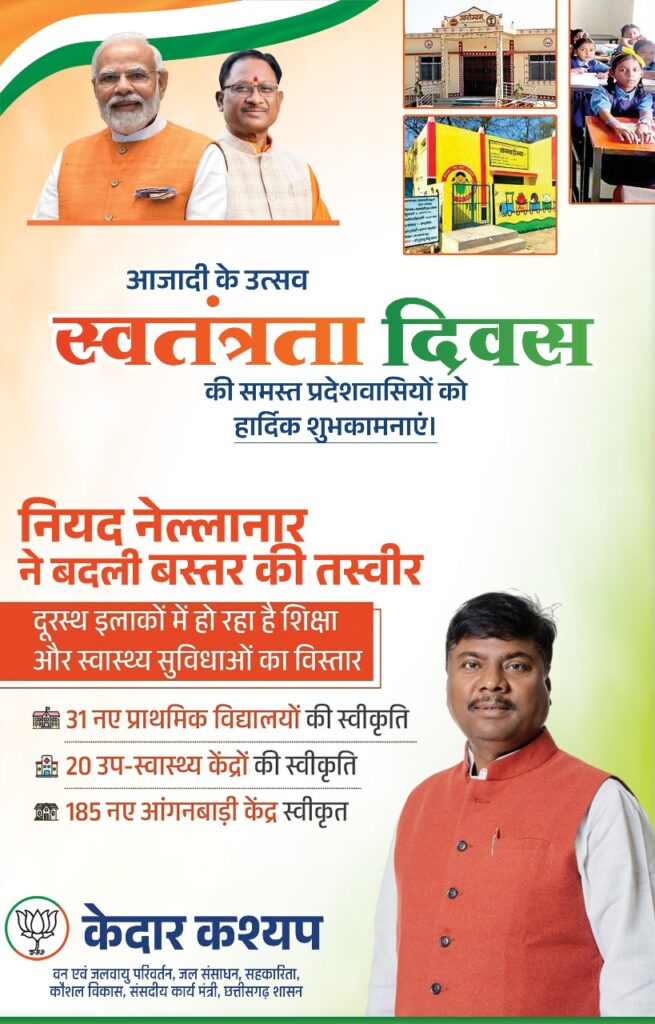



डॉ. हेडगेवार का व्यक्तित्व विराट था। वे क्या गुण थे जो उन्हें अनूठा संगठक बनाते थे ?
वह एक सच्चे स्वप्नद्रष्टा थे। वह भविष्य को देख सकते थे और आने वाले समय का अनुमान लगा सकते थे। वह बहुत विनम्र थे। उनमें अपनी पहचान बनाने या प्रसिद्ध होने की कोई चाह नहीं थी। उनके लिए संगठन ही सब कुछ था और संघ के लक्ष्यों के प्रति वे पूर्णत: समर्पित थे। उन्होंने कभी अपने बारे में या अपनी उपलब्धियों को लेकर बात नहीं की।
क्या संघ को कमजोर करने या खत्म करने के लिए कोई आंतरिक या बाहरी प्रयास हुए ?
संघ के भीतर सभी विषयों पर खुली चर्चा होती है। एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है तो सभी उसका पालन करते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या प्रतिष्ठा के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। संगठन का सामूहिक हित ही सभी का प्राथमिक उद्देश्य होता है। दूसरी विशेषता है स्वयंसेवकों का एक-दूसरे पर *अटूट विश्वास*। तीसरा, स्वयंसेवकों की मान्यताओं में परस्पर अंतर होने के बाद भी उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद न होना। हो सकता है, बाहरी शक्तियों ने संघ को विभाजित या कमजोर करने का प्रयास किया हो, लेकिन अपनी *दृढ़ इच्छाशक्ति* के कारण यह एक अभेद्य दुर्ग बना हुआ है।
क्या संघ को जाति-आधारित भेदभाव या विभाजनकारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा ?
संघ में सभी परंपराओं, पंथों और जातियों के लोग हैं। शाखा बस उन्हीं प्रथाओं का पालन करती है जो इसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हैं। संघ में जाति संबंधित कोई चर्चा कभी नहीं होती। रा.स्व.संघ का सर्वप्रथम यही विचार है कि *हम सभी हिंदू हैं*। जाति की भेद पैदा करने वाली सीमाओं को खत्म करना तभी संभव है जब एक अखंड पहचान बनाई जाए जिसे हम हिंदू एकता कहते हैं। *संघ में जाति का कोई स्थान नहीं है*। जाति उन्मूलन के लिए टकराव का रास्ता जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा देता है। 1974 में अपनी वसंत व्याख्यानमाला के दौरान, तृतीय सरसंघचालक श्री बालासाहेब देवरस ने कहा था, ‘समाज से जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इसका उन्मूलन होना चाहिए, इस बात पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि इससे जाति समाप्त हो जाएगी।’ संघ के कई स्वयंसेवकों ने अंतरजातीय विवाह किए हैं। लेकिन संघ ने कभी भी इन उदाहरणों का प्रचार नहीं किया।
संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार नहीं चाहते थे कि संघ अपनी शताब्दी का उत्सव मनाए। उनके विचारों के प्रकाश में संघ की शताब्दी को आप कैसे देखते हैं ?
डॉ. हेडगेवार ने इच्छा व्यक्त की थी, ‘मैं इसी शरीर में रहते हुए अपनी आंखों से समाज को संगठित देखूं।’(याचि देहि, याचि डोळा अर्थात् इसी देश से और इन्हीं आंखों से) यही कारण है कि संघ ने अपनी पच्चीसवीं, पचासवीं या पचहत्तरवीं वर्षगांठ नहीं मनाई। *पूजनीय सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत ने एक बैठक में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि यह आत्मचिंतन का समय है, आत्मग्लानि का नहीं। जब हम पलटकर अपनी इस यात्रा को देखते हैं तो हमें गर्व के साथ संतोष भी होता है कि हमने यथासंभव वह सब किया जो हम कर सकते थे। लेकिन, इसके साथ ही, किंचित अफसोस भी होता है कि लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए शताब्दी का उत्सव मनाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, संघ के कार्यों को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने, साथ ही इसे और सशक्त करने की योजनाओं और कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है।*
शताब्दी के निमित्त संघ ने दो प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं – शाखाओं की संख्या बढ़ाकर एक लाख करना और पंच परिवर्तन के विचार को क्रियान्वित करना। क्या यह दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत है ?
यह सब संघ की विचारधारा के आधारभूत तत्व हैं। प्रगति की राह में लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य के साथ जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नए द्वार खुलते जाते हैं। *हिंदुत्व कोई अमूर्त आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, जीवन शैली है।* हिंदुत्व का अर्थ अनुच्छेद 370 को हटाना, गोरक्षा या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मात्र नहीं है, जैसा कि आमतौर पर लोग परिभाषित कर देते हैं। *पंच परिवर्तन में निहित सभी बातें हिंदुत्व की प्रतीक हैं।* बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना हिंदू समाज का स्वभाव है। एक जीवंत समाज में समय – समय पर परिवर्तन आवश्यक है। इस दृष्टि से पंच परिवर्तन राष्ट्रधर्म और युगधर्म दोनों से जुड़ा है।
संघ के अनुसांघिक संगठनों को ‘संघ परिवार’ कहा जाता है। क्या ये सभी संगठन अपने आधारभूत उद्देश्यों के अनुरूप समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं ?
संघ ने इन संगठनों का गठन किसी सुनियोजित योजना के तहत नहीं किया है। वास्तव में अपने सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों की भावना और संघ से प्रेरित आदर्शों और अनुभवों के आधार पर अनेक स्वयंसेवकों ने विभिन्न क्षेत्रों में इन संगठनों की स्थापना की है। पिछले 50 वर्ष में स्वयंसेवकों द्वारा स्थापित ये *अधिकांश संगठन संख्या, पहुंच और प्रभाव के मामले में अपने-अपने क्षेत्रों में शीर्ष पर हैं।* ये संगठन अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में काफी सफल रहे हैं।
राजनीति ने न केवल भाषा को बल्कि अन्य कई मुद्दों को जटिल बनाने का काम किया है। संघ इसका समाधान करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है ?
राजनीति के वर्तमान स्वरूप पर मंथन करने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राममनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, पं. मदन मोहन मालवीय और स्वामी संपूर्णानंद जैसे नेताओं की राजनीति संस्कृति पर आधारित थी। हालांकि, उनके अनुयायी इसे वैसा बनाए रखने में विफल रहे, या शायद वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। जबकि सभी दलों का एकनिष्ठ आधार देशभक्ति और राष्ट्रवाद होना चाहिए। देश में बहुत से राजनीतिक दलों की उपस्थिति समाज के लिए बाधा या विभाजनकारी नहीं है। लेकिन राष्ट्र के हित के लिए सबसे आवश्यक है। राष्ट्रीय चेतना का एक सूत्र में बंधना।
संघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करता है। लेकिन क्या आज राजनीतिक सत्ताएं खुद ही संस्कृति के स्वरूप को निर्धारित और नियंत्रित करने में जुटी नहीं दिखतीं ?
हमारे यहां कहावत है – ‘राजा कालस्य कारणम्’ यानी शासक समय का निर्धारण करता है। शासक का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन शासन की श्रेष्ठता उस शासक के सांस्कृतिक आधारों पर निर्भर करती है। राज्य पर संस्कृति का एक अनिवार्य नैतिक प्रभाव बना रहना चाहिए। यही कारण है कि लोकतंत्र और संविधान हमारे समाज के लिए उपयुक्त हैं। कोई भी व्यक्ति केवल अहंकार या स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। आवश्यक है कि समाज और स्वयं को और अधिक सशक्त बनाया जाए। चुनाव और अन्य अवसरों पर अक्सर जनता को बड़े – बड़े वादों और प्रलोभनों से गुमराह किया जाता है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो देश दिवालिया हो जाएगा।
संघ का मानना है कि भारत में सभी नागरिक हिंदू हैं। संघ के ऐसा कहने के पीछे आधार क्या है ?
यह एक स्थापित तथ्य है कि भारत के लोग, चाहे उनकी आस्था, भाषा या परंपरा कितनी ही अलग क्यों न हो, वास्तव में अलग – अलग नस्लों से संबंधित नहीं हैं। हिंदू होना कोई पांथिक पहचान नहीं है। यह एक जीवनशैली है, जैसा कि पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन और यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। उन धार्मिक मान्यताओं को आमतौर पर हिंदू धर्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका पालन हिंदुओं द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका सार मानव धर्म है। भारत के मुसलमानों ने भले अपनी मजहबी मान्यता बदल दी हो। ऐसा हो सकता कि एक बौद्ध कल शायद लिंगायत बन जाए, है न ? एक ब्राह्मण, अगर चाहे तो बौद्ध बन सकता है। हिंदू की अवधारणा कभी भी एक पंथ या परंपरा तक सीमित नहीं रही। दूसरे पंथ को अपनाने मात्र से किसी की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को खत्म करना सही नहीं।
संघ जब कहता है कि मुसलमान और ईसाई हिंदू हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे तभी हिंदू बनेंगे जब वे अपना पंथ छोड़ देंगे ?
किसी को अपना पंथ छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम किसी की उपासना पद्धति का विरोध नहीं करते। शर्त बस इतनी है कि उनकी प्रथाएं इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं के विरुद्ध न हों। बाहरी पंथों के अनुयायियों को भी दूसरों की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
संघ परम वैभव को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है। वे कौन से मील के पत्थर हैं जो यह दर्शाते हैं कि समाज इस आदर्श स्थिति की ओर बढ़ रहा है ?
परम वैभव का सार संघ की प्रार्थना में प्रकट होता ही है, जो समुत्कर्ष (आत्म उन्नति) और निःश्रेयस (मोक्ष) का पाठ पढ़ाता है। इसमें रामराज्य या धर्मराज्य, दोनों शामिल हैं। हम उन लक्षणों की पहचान कर सकते हैं जो इस दिशा में हो रही प्रगति को दर्शाते हैं। सभी को उनकी जरूरत के अनुसार भोजन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव किए बगैर सभी को समान रूप से सामाजिक गरिमा और सम्मान मिलना चाहिए। भारत आज इतना सशक्त हो चुका है कि अपनी धरती और संस्कृति पर होने वाले किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकता है। भारत संकट में पड़े किसी भी समाज, देश या सभ्यता की सहायता करने में भी पूर्ण सक्षम है। यह परम वैभव की ओर बढ़ते समाज के सूचक ही तो हैं।
संघ दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर रहा है, इस अवसर पर आप संघ के स्वयंसेवकों और युवाओं से क्या कहना चाहेंगे?
हम सभी को अपने राष्ट्र की गरिमा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में अपना योगदान देने पर विचार करना चाहिए। उन्हें थोड़ा समय निकाल कर इस दिशा में काम करना चाहिए। हम संकल्प लें कि समृद्धि की ओर अग्रसर भारत को दुनिया के अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश स्तंभ बनाएंगे। स्वयंसेवकों को छोटे-मोटे मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।




